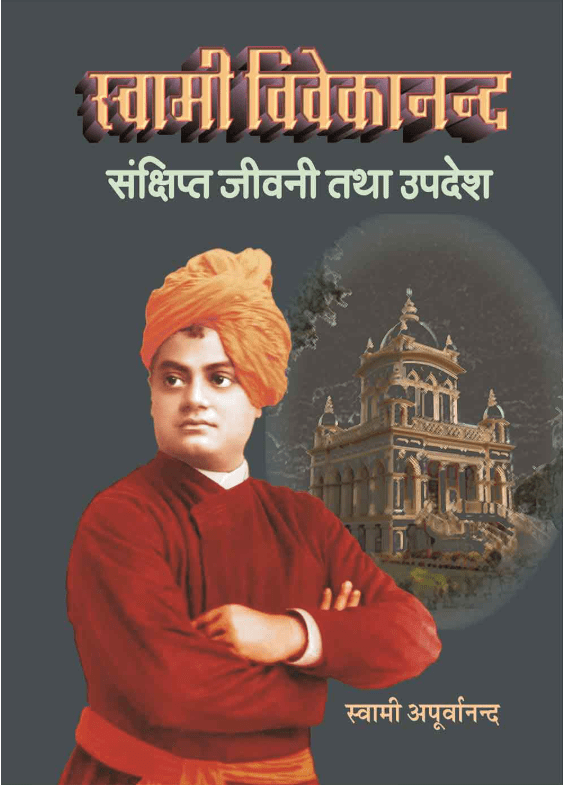23 दिसंबर 2025 का ज्ञानप्रसाद
अमेरिका के मीडिया और जनता ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन (1893) के ऐतिहासिक भाषण और उनकी करिश्माई वक्तृत्व-शैली के कारण “साइक्लोनिक हिन्दू” (Cyclonic Hindu) के विशेषण से सम्मानित किया था। वे एक बवंडर (cyclone) की तरह अपनी ऊर्जा, ज्ञान और भारतीय दर्शन की प्रस्तुति से पश्चिमी दुनिया को झकझोर गए थे, जिससे लोग चकित रह गए और उन्हें यह उपनाम दिया गया, जिसका अर्थ था एक प्रभावशाली, ऊर्जावान और क्रांतिकारी हिंदू साधु। उस Cyclone का ही प्रभाव है कि 133 वर्ष बाद भी उनकी वाणी एवं विचार ऑनलाइन ज्ञानरथ गायत्री परिवार के साथिओं की आत्मा को झकझोड़ रहे हैं। एक-एक लेख,एक-एक शब्द में जो ज्ञान भरा पड़ा है उसे केवल आत्मा के स्तर पर ही अनुभव किया जा सकता है।
लेख को लिखते समय अनेकों स्थान पर उत्कृष्ट विचारों को Commas से हाईलाइट किया हुआ है,साथिओं से निवेदन करते हैं कि प्रत्येक ज्ञानप्रसाद की भांति इसे भी आत्मसात करते हुए अपने ह्रदय में उतारने का प्रयास करें।
लेख का शुभारम्भ अर्थ सहित शांतिपाठ से होता है :
ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षँ शान्ति:,पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:।वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति:,सर्वँ शान्ति:, शान्तिरेव शान्ति:, सा मा शान्तिरेधि॥ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥
अर्थात शान्ति: कीजिये प्रभु ! त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में,अन्तरिक्ष में, अग्नि – पवन में, औषधियों, वनस्पतियों, वन और उपवन में,सकल विश्व में अवचेतन में,शान्ति राष्ट्र-निर्माण और सृजन में, नगर , ग्राम और भवन में प्रत्येक जीव के तन, मन और जगत के कण – कण में, शान्ति कीजिए ! शान्ति कीजिए ! शान्ति कीजिए
***********
उत्तर भारत में कुछ भागों का पर्यटन करते समय उनके सम्मुख प्राचीन भारत, वर्तमान भारत तथा भावी भारत का चित्र उज्ज्वल रूप से झलमला उठा तथा साथ ही उनकी पैनी/दिव्य दृष्टि के सामने विश्वमानवता(Universal humanism) का एक नया रूप प्रकट हुआ।
स्वामी जी की अंतरात्मा में जिस “सनातन वैदिक भारत” की छवि उभर कर आयी उन्होंने निम्नलिखित भारत को देखा:
पुराण, इतिहास एवं Legends की अगणित महिमा से मण्डित देवी-देवताओं वाला भारत
एकता, मैत्री और स्वाधीनता का सन्देश सुनाने वाली सभ्यता की आधारशिला पर प्रतिष्ठित, आर्य-द्रविड़ आदि अनेक सम्यताओं की मिलन भूमि भारत
Prehistoric काल से लेकर आज तक जाति-वर्ण-धर्मनिरपेक्ष रूप से सभी देशों के लोगों को निडरता का आश्रय देते हुए अपने हृदय में बसा लेने वाला भारत
विश्वमानवता की जन्मभूमि भारत।
स्वामीजी ने वराहनगर मठ में लौटकर अपने गुरुभाइयों को अपनी अंतरात्मा में उठ रही भावधारा का सहभागी बनाया।
कुछ समय वराहनगर मठ में निवास करने के पश्चात् जुलाई 1890 में स्वामीजी ने पुनः हिमालय की यात्रा की। साथ में पथ-प्रदर्शक के रूप में उनके गुरुभाई स्वामी अखण्डानन्द थे, जो तिब्बत तथा हिमालय-भ्रमण के अनुभवी थे। पहले वे भागलपुर, वैद्यनाथ और काशी गये | तरुण भास्कर के समान वे अपनेआप को कहीं भी छिपा न पाए । जिस किसी ने क्षण भर के लिए भी उनके साथ वार्तालाप किया, वही उनके भीतर निहित महाशक्ति का परिचय पाकर मुग्ध हो उठा। वे केवल गेरवे वस्त्रधारी, मुण्डित-मस्तक यति (सांसारिक मोहमाया से विरक्त) ही नहीं थे, वे तो साक्षात् अग्नि के अंगारे थे। उनके नेत्रों में प्रतिभा का जो तेज झलकता था, उसे वे किसी भी प्रकार ढक नहीं सकते थे ।
यथाक्रम उन्होंने नैनीताल, अल्मोडा, ऋषिकेश, कनखल, सहारनपुर, मेरठ आदि स्थानों पर गुरुभाइयों के साथ कठोर तपस्या में कालयापन किया। इस समय उन्होंने अपने भीतर “एक महाशक्ति के कंपन ” का अनुभव किया और उन्हें अपने जीवन के महान् कर्तव्य के सम्बन्ध में संकेत मिला। अपने संकल्प में दृढ़ हो उन्होंने एक दिन अपने साथ के गुरुभाइयों को बुलाकर कहा-
“मेरे जीवन का व्रत स्थिर हो चुका है। अब से मुझे बिलकुल अकेले रहना होगा। तुम लोग मेरा साथ छोड़ दो। मेरे साथ एकमात्र भगवान् ही रहेंगे।”
उन्होंने गुरुभाइयों का कोई अनुरोध नहीं सुना। मात्र 6 माह में ही, जनवरी 1891 के अन्तिम दिनों में वे एकाकी परिव्राजक (Lonely traveler) के रूप में निकल पड़े और भारत के विशाल जनसमुद्र में विलीन हो गये। अन्य सैकड़ों गेरुआ-धारी संन्यासियों की तरह वे भी एक संन्यासी मात्र थे। दो वर्ष से भी अधिक काल तक वे इसी प्रकार भ्रमण करते रहे। भारतभूमि के धूलिकणों में उनके पदचिह्न विलीन होते गये। वे कभी ग्राम में, कभी नगर में, कभी धनिक के भवन में, कभी दीन की कुटीर में,कभी उच्चवर्ण ब्राह्मण के सम्मानित अतिथि के रूप में, कभी अस्पृश्यों को धन्य करते हुए उनके सुख-दुःख के सहभागी के रूप में, कभी राजा-महाराजाओं के महलों में मान्यवर संन्यासी गुरु के रूप में उच्च आसन पर विराजमान होते रहे। राजागण उनके चरणों की सेवा करते। भोगविलास से ओतप्रोत राजाओं के हृदय में वे ज्ञानलोक की बाती जलाते हुए, लोगों को बताते रहे कि यह संसार अस्थिर है, अनित्य है, हमेशा बदलता रहता है। स्वामी जी जहाँ भी गए,उन्होंने लोगों के सोये हुए हृदयों में जनता-जनार्दन की सेवा की चेतना जगाने का प्रयास किया। तब एक स्टेज ऐसी आ गयी कि लोगों ने उन्हें पीड़ितजनों के मित्र के रूप में, वेदनापूर्ण प्राणों से उनकी सेवा में निमग्न प्राणी के रूप में पाया।
जैसे-जैसे दिन बीतते गये वैसे-वैसे उनके हृदय में इस महान् भारतभूमि का वास्तविक रूप स्पष्ट दिखने लगा। उन्होंने देखा कि भारत में मानव के भीतर भगवान् किस तरह दुःख और क्लेश से व्यथित बने हुए हैं। भारत की अपार जनता की करुणाभरी पुकार से वे कैसे व्याकुल हो उठे, उसे हम सब पाठक भलीभांति अनुभव कर रहे हैं।
मेरठ से स्वामीजी दिल्ली आये। वहाँ से अलवर होते हुए जयपुर में दो सप्ताह रहे। जयपुर और उसके आसपास सर्वत्र जनसाधारण की निर्धन और असहाय दशा देखकर स्वामीजी का हृदय वेदना से भर उठा। भारत देश के निर्धन,दीन जन नारायणों की शोचनीय परिस्थिति को सुधारने की दिशा में वे राजाओं और राजकर्मचारियों को प्रोत्साहित करने लगे।
इन्हीं निर्धन,अशिक्षित जन नारायणों को स्वामी जी ने भारत का मेरुदण्ड यानि रीढ़ की हड्डी कहा,इन्हें ही राष्ट्र के प्राण कहा एवं भारत के भविष्य को तय करने के लिए वे नवयुवकों को प्रेरणा देने लगे। इस दलित और पीड़ित जनता के साथ स्वामी जी के सम्पर्क जितने भी घनिष्ठ होते गए, उनके अंतर्मन में जनसेवा का व्रत उतना ही स्पष्ट आकार धारण करने लगा। उनकी समस्त शक्ति एवं चेष्टा, मानव की पीड़ा और व्यथा को केन्द्रित करके ही नर-रूपी नारायण की सेवा में लगी थी। उन्होंने कहा था:
“मैं एक ऐसा धर्म (मानव धर्म) चाहता हूँ जो हम में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बोध जगा दे तथा हम में दीन-दुखियों को अन्न और शिक्षा देने की, एवं हमारे चारों ओर फैले समस्त दुःख कष्टों को दूर करने की शक्ति भर दे। यदि ईश्वर से लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले मनुष्य की सेवा करो।”
जनसेवा के व्रत में उन्होंने अपने हृदय की सारी शक्ति उड़ेल दी। “समस्त विश्व के दीन-दुखियों का हृदयभेदी हाहाकार उनके अंतर्मन में प्रतिध्वनित हो उठता।” इसीलिए उन्होंने सर्वत्र “नररूपी नारायण” की सेवा का मंत्र सुनाया। भारत के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक सभी लोगों को नरनारायण- सेवाव्रत के सन्देश से अनुप्राणित किया। नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्राणों में स्वामीजी के इस सन्देश ने विलक्षण झंकार उठायी थी। वे लिखते हैं:
“विवेकानन्द ने कहा था दरिद्र नारायणों के माध्यम से परमात्मा हमारी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। इसे कहते हैं सन्देश ! इस सन्देश ने स्वार्थबोध के परे मनुष्य के आत्मबोध को असीम मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह किसी आचार-विशेष का उपदेश नहीं है। यह कोई व्यवहारोपयोगी संकीर्ण अनुशासन नहीं है। छुआछूत को रोक पाना इसमें अपनेआप ही आ जाता है इसलिए नहीं कि उसके द्वारा राष्ट्र के स्वतन्त्र होने का सुयोग है, बल्कि इसलिए कि उसके द्वारा मनुष्य का अपमान दूर होगा। वह अपमान हममें से प्रत्येक पर लांछन है। विवेकानन्द का यह सन्देश सम्पूर्ण मानवजाति के लिए मार्गदर्शक है और इसलिए वह हमारे युवकों को कर्म के माध्यम से मुक्ति के विभिन्न मार्गों की ओर प्रवृत्त कर रहा है।”
भारत की आम जनता की दुर्गति देखकर स्वामीजी का हृदय अत्यन्त दुखित हो गया था। केवल भारत ही नहीं, सभी देशों की सभी जातियों के लिए उनके प्राण रोया करते थे। उनके विशाल हृदय में किसी प्रकार की भौगोलिक सीमा नहीं थी। उन्होंने कहा था:
“भगवान् को किधर ढूँढ़ते फिर रहे हो? क्या दीन,घृणित,अछूत तुम्हारे देवता नहीं हैं? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? … वेदान्त की जन्मभूमि भारतवर्ष में साधारण जनता का युग-युग से अपमान होता आया है।अस्पर्शों का स्पर्श धर्म के विरुद्ध है, उनका संग अपवित्र है। निराशा के अन्धकार में उनका जन्म होता है, उसी में उनकी निरन्तर स्थिति है। याद रखो, निर्धन की कुटिया में ही भारतीय राष्ट्र बसता है। किन्तु हाय! उनके लिए अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। अनादर सहते, भारत के उपेक्षित किसान, जुलाहे, चमार, झाडूदार आदि निम्न श्रेणी के लोग, उच्च श्रेणी द्वारा उत्पीड़ित हुए जा रहे हैं। तथा स्वदेश-वासियों की अवज्ञा के बावजूद वर्षों से चुपचाप रहकर अपना काम करते आ रहे हैं; इसके लिए उन्होंने कभी उपयुक्त वेतन तक नहीं पाया ।”
इस व्यथा में विवश, कमण्डल-धारी परिव्राजक के वेश में स्वामीजी चलते गये। उन्होंने आबू पर्वत के रमणीक वातावरण के बीच 13वीं शताब्दी में आठ करोड़ रुपयों से निर्मित अनुपम बेलबूटों से सुशोभित जैनमन्दिर का दर्शन किया।
आबू में रहते समय स्वामीजी का खेतड़ी के महाराजा से परिचय हुआ। महाराजा के विशेष आग्रह पर स्वामीजी उनके साथ खेतड़ी आये और कुछ दिन वहाँ निवास किया। यहाँ पर स्वामीजी केवल राजमहल की सुख सुविधा का आनंद ही नहीं उठाते रहे। वे प्रजा के सुख-दुःख के भी सहभागी हुए। राजपूताना के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते समय ही वे दीन-दुखियों की हृदयद्रावक शोचनीय दशा के साथ विशेष रूप से परिचित हुए। उन्होंने इसके निवारण की चेष्टा भी की। उन्होंने राजा-महाराजाओं के हृदय में जनसेवा का भाव जगाया। स्वामीजी के उपदेशों से अनुप्राणित हो खेतड़ी नरेश ने अपने राज्य में जनता के विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं बनाईं।
राजाओं के हाथ में शक्ति थी,धन था, इसीलिए स्वामीजी उनसे मिलकर उनके मन में परिवर्तन लाना चाहते थे। वे जहाँ कहीं भी गये, वहीं उन्होंने धनिकों के समीप निर्धनों के कल्याण के लिए आवेदन किया। परन्तु वे यह भी समझ चुके थे कि केवल दो-एक राजा- महाराजाओं की दानशीलता और सदिच्छा से भारत के व्यापक दुःख दैन्य में केवल मामूली सा ही सुधार हो सकता है। स्वामीजी की पाश्चात्त्य देश जाने की कल्पना के पीछे कुछ अंश में भारत के इस दुःखमोचन का भी उद्देश्य था। उन्होंने कहा था:
“मैंने समूचे भारत का भ्रमण किया । … अपनी आंखों से सर्वत्र ही आम जनता का भयावह दु:ख दैन्य देखा। वह सब देखकर मैं व्याकुल हो उठा हूँ। मेरी आँखों के आँसू रोके नहीं रुकते। इसी कारण, जनसाधारण की मुक्ति का कोई उपाय ढूँढ़ निकालने के लिए मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ। “
खेतड़ीनरेश के आग्रहपूर्ण प्रार्थना करने पर भी स्वामीजी खेतड़ी छोड़कर गुजरात चले गये। अहमदाबाद, लिमड़ी, जूनागढ़, गिरनार, भुज, वेरावल और सोमनाथ होते हुए वे पोरबन्दर (सुदामापुरी) पहुँचे। पोरबन्दर के महाराजा के साथ स्वामीजी का परिचय इतना घनिष्ठ हुआ कि स्वामीजी ने लगभग आठ-नौ महीने राजभवन में ही निवास किया। इस दीर्घकाल निवास का विशेष कारण भी था। राजा के सभा पण्डित शंकर पाण्डुरंग असामान्य विद्वान् थे। वे उस समय वेदों का अनुवाद कर रहे थे। उनके अनुरोध पर स्वामीजी उन्हें अनुवाद कार्य में सहायता किया करते थे।
आज के लेख का यहीं पर मध्यांतर होता है।
धन्यवाद्,जय गुरुदेव